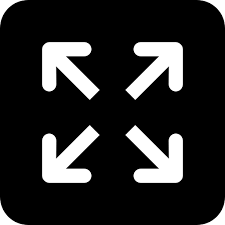जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात
वक्त को हाथ से मत निकलने दीजिए
पिछले साल अक्टूबर में नरेन्द्र मोदी सरकार ने अचानक सदाशयता दिखाते हुए कहना शुरू किया कि वह कश्मीर की समस्या का सभी सम्बद्ध पक्षों से बातचीत की मार्फत समाधान चाहती है, तो देश उसकी ओर से इस दिशा में किसी बड़ी राजनीतिक पहल की उम्मीद करने लगा था। उसने एक कदम और आगे बढ़कर आईबी के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा को, जो पहले भी कश्मीर में काम कर चुके हैं और समस्या की प्रायः सारी पेचीदगियों से वाकिफ हैं, अपना वार्ताकार बनाने का फैसला किया तो कई हलकों में नयी उम्मीदों का सैलाब-सा आ गया था। शर्मा ने भी यह कहकर इस सैलाब को और बढ़ाया ही था कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर, खासकर घाटी के युवाओं को डि-रेडिकलाइज करना होगी।
उनकी यह प्राथमिकता अमल में आती तो निश्चित ही लम्बे अरसे से आतंकवाद और अलगाववाद से पीड़ित इस सीमावर्ती राज्य के निवासियों की दुखती रगों को थोड़ा सुकून मिलता, जो उसकी समस्या के समाधान की ओर प्रस्थान की पहली और अनिवार्य शर्त है। वे उन युवाओं को ठीक से सम्बोधित करते, क्रूर आतंकवाद ने जिन्हें त्रासद वर्तमान के साथ अंधे भविष्य से भी अभिशापित कर रखा है, तो कोई कैसे कह सकता है कि अच्छे नतीजे नहीं निकलते? धरा का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर की धरती पर फिर जहन्नुम का नंगा नाच क्यों कर जारी रहता?
लेकिन विडम्बना यह कि दिनेश्वर शर्मा अपनी नियुक्ति के छः-सात महीनों बाद भी अपनी प्राथमिकता के पहले पायदान तक पर नहीं चढ़ पाए हैं, जबकि कश्मीर के हालात खासी तेजी से खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। इस बीच जो सबसे खराब बात हुई है, वह यह कि जम्मू और कश्मीर के बीच का साम्प्रदायिक विभाजन अपने नग्नतम रूप में सामने आ खड़ा हुआ है। हालत यह है कि एक सम्प्रदाय की बच्ची दूसरे सम्प्रदाय के वहशियों की शिकार हो जाती है तो दूसरे सम्प्रदाय के ठेकेदारों को अपने वहशियों के बचाव में तिरंगे झंडे फहराते और भारतमाता की जय बोलते भी शर्म नहीं आती।
तिस पर हालात से निपटने को लेकर केन्द्र व जम्मू कश्मीर की सरकारों का परस्परविरोधी रवैया कोढ़ में खाज की स्थिति पैदा कर रहा है। चूंकि यह कोढ़ में खाज तब गुल खिला रहा हैं, जब दोनों सरकारों के एक दूजे की शुभचिंतक होने के कारण लोग उनसे समन्वय के साथ काम करके राज्य को अमन और खुशहाली की ओर ले जाने की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए अब उम्मीदों की जगह निराशाओं ने ले ली है। कई हलकों में तो निराशाओं का कुछ ऐसा जोर है कि एक वरिष्ठ सम्पादक ने यह लिखने से भी परहेज नहीं किया है कि कुछ सदियों बाद जब हमारा नया इतिहास लिखा जाएगा, तो शायद यही लिखा जायेगा कि जम्मू-कश्मीर जल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे।’ साफ है कि उनके लापरवाह रवैये को लेकर लोगों को ‘रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था’ जैसी कहावत याद आ रही है।
बहरहाल, रोम को जलता देखने वाले अब नहीं हैं, लेकिन हम रोज ही कश्मीर को जलता-झुलसता देख रहे हैं, जबकि कई और मामलों में इतिहास रचने को बेताब प्रधानमंत्री ने, लगता है, उसकी समस्या के हल को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में कहीं रखा ही नहीं है। इस कारण निराशाओं का बढ़ना बहुत स्वाभाविक है, फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि प्रधानमंत्री इतिहास में नीरो की तरह नाम दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन इस बात का क्या किया जाये कि उनकी चार सालों की सत्ता के बाद कश्मीर में जैसे हालात उत्पन्न हो गये हैं, वैसे उसके इतिहास में पहले शायद ही कभी पैदा हुए हों।
जहां तक आतंकवाद की बात है, वह तो वहां बीते 3-साढ़े 3 दशकों से है, पर उसे लेकर आम कश्मीरी ने इससे पहले कभी खुद को इतने संदेहों के दायरे में नहीं पाया। विडम्बना देखिये कि न केन्द्र और न ही जम्मू कश्मीर की सरकार यह समझ पा रही है कि वे राज्य के समूची जनता को पाकिस्तान या उसके पाले आतंकियों के बहकावे में आ गई मानकर आतंकवाद के उन्मूलन में नहीं प्रमोषन में ही सहायक हो रही हैं। और तो और, उनके पास इस सवाल का जवाब भी नहीं कि वहां बंदूकों व बमों के साथ पत्थर भी कब, क्यों और कैसे आतंक के हथियार बन गए? जैसे भी बन गये हों, बन ही गये हैं तो अब सारे कश्मीरियों को पत्थरबाज कहकर चिढ़ाने से बात बनेगी, सेनाध्यक्ष द्वारा यह कहकर धमकाने से कि वे किसी भी हालत में सेना से नहीं लड़ पायेंगे या गंभीरता से उनका खोया हुआ विश्वास फिर से जीतने की कोशिशें करने से?
मुश्किल यह है कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग ‘घोषित’ करते रहने से आगे बढ़ ही नहीं पा रही, जबकि जरूरत कश्मीरियों के जख्मों की टीस महसूस करने की है। वहां के नाजुक हालात में सद्भावना की जरूरत को पूरी तरह दरकिनार करके बोली के बजाय गोली की विचारधारा का ही नतीजा है कि वहां के उन युवकों के हाथों में भी पत्थर आ गये हैं, जो पहले शांतिकामी हुआ करते थे। अब सुरक्षा बल ही नहीं आम नागरिक भी उनके निशाने पर आ गए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने मासूम बच्चों से भरी स्कूल बस पर पत्थर मारे थे। फिर पर्यटकों की एक बस पर हमला कर चेन्नै के एक पर्यटक को मार डाला। इससे पहले भी उन्होंने करीब आधा दर्जन पर्यटकों को चोटें पहुंचाई थीं। सवाल है कि क्या इन पत्थर मारने वालों वालों को इतना भी नहीं मालूम कि ये पर्यटक ही जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं? अगर नहीं तो उन्हें यह बताना किसकी जिम्मेदारी है और मालूम होने के बावजूद उन्होंने यह आत्मघाती राह चुनी है तो क्या उनके गुस्से या भटकाव को समझे बगैर समस्या का कोई समाधान निकल सकता है? लेकिन इस सवालों से जूझे कौन, जब केन्द्र या राज्य सरकार के पास उनसे जुड़ा कोई विचार, योजना या दूरदृष्टि है ही नहीं-केवल भावनाओं को भुनाने वाले मुद्दे हैं, जो पाकिस्तान को सबक सिखाने, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने, धारा 370 हटाने व समान नागरिक संहिता लागू करने जैसी तोतारटंतों के इर्द-गिर्द घूमते रहते हंै।
ये सरकारें चाहती है कि शेष देश भी ऐसी ही उथली चर्चाओं में लगा रहे, जबकि जरूरत इन सवालों के रूबरू होने की है कि वह कौन-सी नाइंसाफी है, जिसे न सह पाने के कारण कश्मीरी युवक कभी पत्थर तो कभी बंदूक उठा रहे हैं? फिर उनके मां-बाप उन्हें बरजने के बजाय इस रास्ते पर क्यों बढ़ने देते हैं? किसी आतंकी की मौत होते ही उसकी खबर को कुछ चैनलों में ग्लैमराइज करके दिखाने के पीछे कौन-सा एजेंडा काम करता है? कश्मीर के कुछ बच्चे क्रिकेट या सिविल सर्विसेस एग्जाम्स में सफल हो जाते हैं, तो क्या इससे बाकी बच्चों का भविष्य भी संवर जाता है? वहां की नयी पीढ़ी के लिए शिक्षा और रोजगार के बेहतरीन अवसर जुटाने की क्या योजना है? सरकार पाकिस्तान पर इल्जाम लगाती है कि वही कश्मीर में आतंकवाद का प्रायोजक है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि क्यों वह पाकिस्तान के आगे लगातार बेबस साबित हो रही है? क्यों वहां युद्धकाल से भी ज्यादा जवान और आम नागरिक हताहत हो रहे हैं? वहां सेना ऐसे ही इंसान को ढाल की तरह इस्तेमाल करने जैसे पैंतरे आजमाती रही तो सुरक्षाबलों और आम लोगों के बीच अविश्वास की खाई कैसे पटेगी?
ये सवाल अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन इनके उत्तर तलाशे बगैर कश्मीर समस्या का समाधान मुमकिन नहीं है। बेहतर हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बात को समझें और पिछले चार सालों में अपनी कश्मीर सम्बन्धी नीति या अनिर्णय से जनमी असफलताओं व निराशाओं से सबक लेकर परस्पर विश्वासबहाली की नयी पहलें करें। ऐसी पहलों के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। अलबत्ता, और देर की गई तो वक्त हाथ से निकल सकता है।