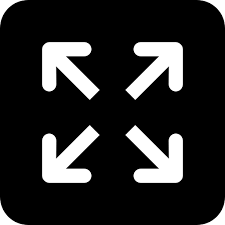लोक में भटकते मुद्दे और आम चुनाव
राष्ट्रवाद की आड़ में जनहित के असल सवाल बहस से बाहर
लोकसभा के आम चुनावों के दौरान लोक जीवन को अधिकता से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जद्दोजहद होना एक आम चलन है। राजनीतिक लोकतंत्र में जन विश्वास और मोह बनाये रखने के लिए यह बेहद जरूरी है । और यह प्रक्रिया पहले आम चुनाव से लेकर आज तक जारी है । पिछले कई चुनावों से लोक प्रश्नों पर राजनीतिक मंथन की प्रक्रिया में ऐसे सवाल अधिक दिखाई देने लगे हैं, जो राजनीतिक बिसात बिछाने में सहायक रहते हैं। इससे लोकहित के मुद्दों पर विमर्श या सत्ता से सवाल पूछने की अपेक्षा समाज का विभाजन किसी खास जाति, धर्म, भाषा या इलाके के आधार पर होने लगता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान लोकतंत्र का, फिर समाज और समुदाय का होता है और सरकार बनाने वाला दल उस जनसमूह का राजनीतिक शोषण करने के बाद बार-बार ऐसे मुद्दों को उठाने की योजना बनाता रहता है। ऐसा होना किसी भी समाज की विकास संबंधी धारणा, राजनीतिक जागरूकता और उसकी सांस्कृतिक समझ पर निर्भर करता है। जिस देश, समाज और सांस्कृतिक समूह में अपने सामाजिक सरोकारों को भूलकर ऐसे हवा-हवाई मुद्दों से राजनीतिक जुड़ाव हो तो निहित स्वार्थों को फायदा मिलता है। भारतीय राजनीति में विकास एक ऐसा शब्द हो गया है जिसका दुरूपयोग अधिक हुआ है और कोई भी दल या नेता विकास की प्रक्रिया को समझे बगैर विकास-विकास के नारे लगाने लगता है। वर्तमान राजनीतिक लोक में यह एक सेट फार्मूला बन चुका है जो पहले के विकास को झूठलाकर खुद आगे हो जाता है । लेकिन हम सार्वभौमिक विकास से अभी बहुत दूर हैं ।
पिछले दस साल में विकास के गुजरात मॉडल की चर्चा होती रही है. इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने को चुनावी मुद्दा बनाकर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया और चुनाव के बाद उसे लागू करते हेतु राजकीय क्षेत्र का निजीकरण करने की प्रक्रिया के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 51 प्रतिशत से अधिक कर दी गई। राजकीय क्षेत्र का निजीकरण संविधान के कल्याणकारी संकल्पों के खिलाफ है, लेकिन लोकहित को छोड़कर जनता को गुमराह करने का अभियान फिर से जारी है । गुजरात मॉडल की चर्चा अब कहीं मीडिया और जनता में नहीं है । इससे मालूम होता है कि जनता को बरगलाने के लिए यह मुद्दा सामने किया गया था और अब इसकी कलई खुल चुकी है।
लोक हित के असल सवालों यानी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा व प्रतिनिधित्व जैसे मूलभूत प्रश्नों को अब राष्ट्रवाद और उससे आगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आड़ में विचार और बहस से बाहर किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि कुछ समय से चुनावी सभाओं में असली राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद, असली ओबीसी और नकली ओबीसी, सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण के साथ-साथ सर्वोच्य न्यायालय के सबरीमाला निर्णय, बिलकिस बानो निर्णय, राफेल भ्रष्टाचार संबंधी मामला, सर्वोच्य न्यायालय द्वारा सीबीआई को पिंजरे का तोता जैसे कथन, राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक निकायों की कार्य प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप, निर्वाचन आयोग द्वारा आचार सहिंता उल्लंघन संबंधी मामलों में पक्षपात के आरोप जैसे सवाल निरंतर सामने आए हैं। यदि लोकतंत्र में जनता को न्याय नहीं मिलता तो फिर जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार का क्या अर्थ रह जाता है?
बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि “राजनीति में भक्ति या नायक पूजा शर्तिया तौर पर समाज के पतन और उसे संभावित तानाशाही की ओर ही ले जाती है।’’ उन्होंने सामाजिक अंतर्विरोधों को रेखांकित करते हुए कहा था कि “26 जनवरी 1950 को हम राजनीतिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य को लागू करेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति एक मूल्य को नहीं मानेंगे। यदि सरकार ने इस असमानता को समाप्त करने के लिए सार्थक प्रयास नहीं किए, तो शोषण के शिकार लोग इस राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे।’’ असल में, वे ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां साथी नागरिकों के प्रति समानता का व्यवहार करने वाला सामाजिक लोकतंत्र बने। इसलिए हमें राष्ट्रवाद की बहसों में समय लगाने की बजाय या समाज को गुमराह होने से बचने के लिए संविधान निर्देशित राजकीय क्षेत्र में समुचित हिस्सेदारी और अवसरों की समानता के मुद्दे उठाने में और देरी नहीं करनी चाहिए। काले धन, भ्रष्टाचार, धार्मिक अल्पसंख्यकों, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, महिलाओं का शोषण, नोटबंदी, जीएसटी का मामला, राजकीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, खेती और किसानी, स्मार्ट सिटी बनाने जैसे सवाल अभी चुनावी बिसात से गायब हो रहे हैं। इन प्रश्नों पर देश सत्ता के मन की नहीं, अपनी बात कहते हुए सबका साथ सबका विकास देखना चाहता है।
यदि सरकारों ने सामाजिक शोषण और संविधान को दरकिनार करके बाजारपरस्ती की नीतियां नहीं बदलीं, तो देश आंतरिक अशांति और गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 131 सांसद (87+47 कुल 24.12 प्रतिशत) तथा 30 राज्य विधानसभाओं के लिए चुने जाने वाले1169 विधायक (613+556 कुल 28.37 प्रतिशत) पीड़ित वंचित समाज की आवाज उठा पाने में नाकाम रहे हैं। इनकी चुप्पी इनके ऊपर बड़े दबाव की सूचक और प्रतिनिधित्व के लिए खतरे की घंटी हो सकती है।
लोक सभा के मुद्दे जनता के सरोकारों से जुड़े हुए होने चाहिए । यदि मीडिया किसी खास स्वार्थ में जन सरोकारों को सामने नहीं ला रहा है, तो निश्चित रूप से जन सरोकारों वाले वैकल्पिक मीडिया को आगे आना होगा और इसमें सोशल मीडिया भी अहम भूमिका निभा सकता है।